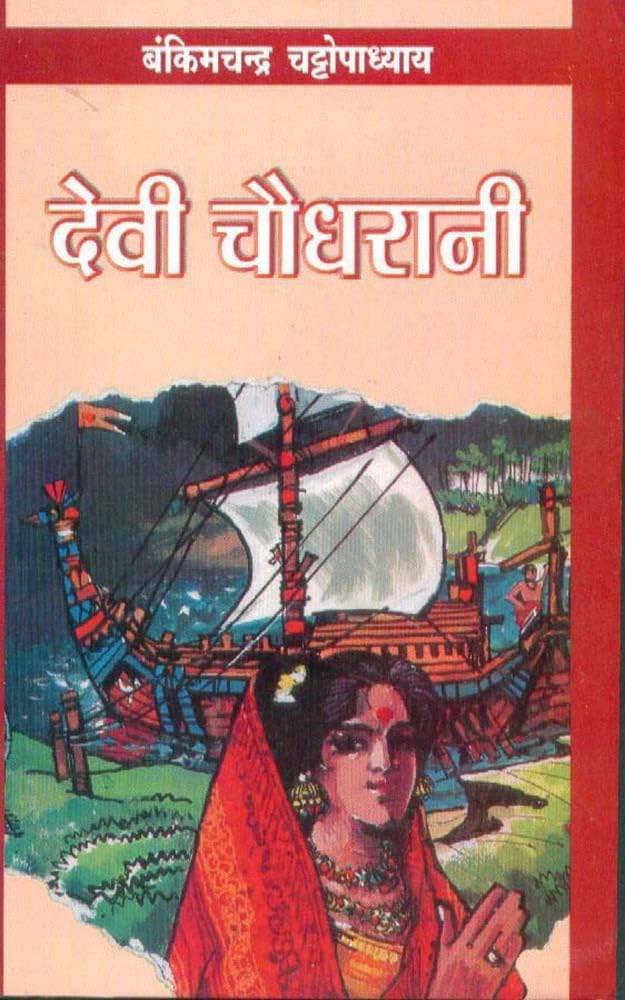पब में

पब की बुझी-बुझी सी रोशनी,
काँच के गिलासों की खनक,
कहीं दूर से आती बेफ़िक्र हँसी,
और फिर, सामने की मेज़ पर—
तुम।
काले लिबास में लिपटी,
खुली ज़ुल्फ़ों में उलझी,
तुम्हारी आँखें टिमटिमाती हैं,
जैसे अंधेरे आकाश में
कोई भूला हुआ सितारा चमका हो।
एक पल के लिए,
हमारी नज़रें मिलती हैं—
तुम मुस्कुराती हो
और मेरी धड़कन,
तेज़ हो जाती है,
जैसे बरसों पुरानी धुन
फिर सुन ली हो।
एक आवाज़ भीतर से कहती है—
"उठो,
चलो,
उस तक जाओ।
शायद नाम पूछो,
कोई नया किस्सा शुरू करो।"
मगर तभी
यादों के बादल
फिर से छा जाते हैं।
वो पुराने चेहरे,
टूटे वादे, बिखरे रिश्ते—
सब एक-एक कर
मेरी मेज़ पर
बैठ जाते हैं।
वही परिचय, वही कशिश,
मीठे लम्हों के बाद
वही बहस, वही तकरार।
वही आँसू, वही सवाल—
"गलती आख़िर थी किसकी?"
फिर अकेलेपन की ठंडी दीवार,
वही दोहराव,
एक थकी-हारी फ़िल्म
जो बार-बार रिवाइंड हो रही है,
हर दृश्य मुझे ज़ुबानी याद है।
तुम फिर देखती हो—
इस बार कुछ देर तक,
शायद उम्मीद से।
मैं नज़रें फेर लेता हूँ,
कोई अपराधी-सा,
पकड़े जाने के डर से।
क्योंकि इस दिल में
अब एक नई कहानी का
सामर्थ्य नहीं।
शायद कभी था भी नहीं।
मैं सोचता हूँ—
एक और घूँट ले लूँ,
शायद ये अधूरी ख़्वाहिश
इस शराब के साथ
हल्की होकर बह जाए।
तुम उठती हो,
अपने दोस्तों के साथ जाने को।
एक आख़िरी बार देखती हो,
शायद थोड़ी मायूस,
थोड़ी उलझन के साथ।
और मैं वहीं बैठा रहता हूँ—
अपनी मेज़ पर,
किसी बुत की तरह
जिसे आदत हो गई है
खुद को भूल जाने की,
इस भीड़ भरे पब की
मद्धम रोशनी में।
(यह कविता शराब‑-सेवन को बढ़ावा नहीं देती; अत्यधिक मदिरापान स्वास्थ्य ‑के लिए हानिकारक है।)
रचना शेयर करिये :