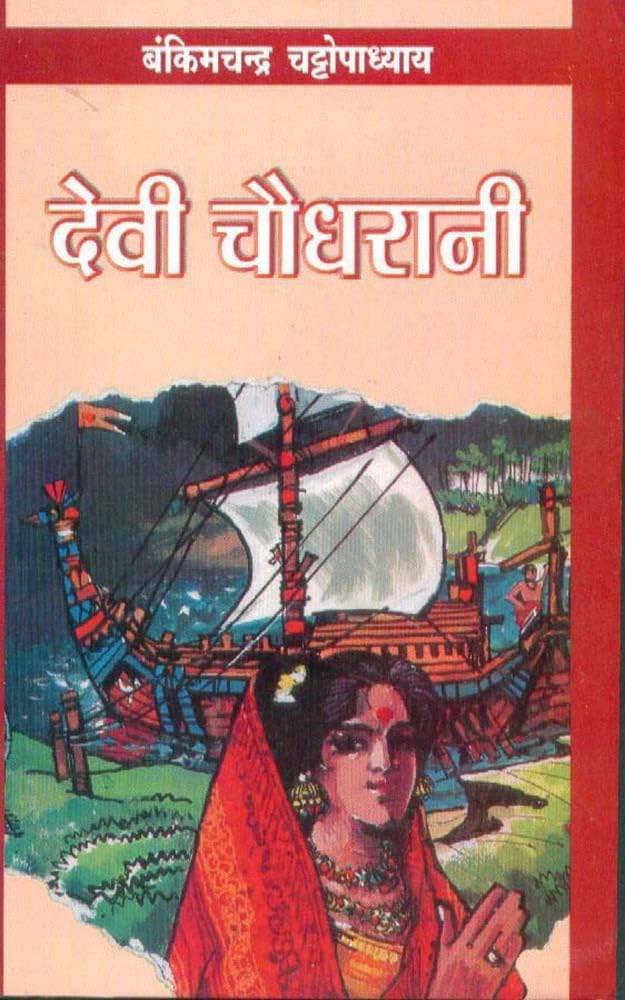पिताजी का ग़ुस्सा

पिताजी का ग़ुस्सा,
जैसे अचानक बादल गरज उठे
गर्मी के दिन में।
हम सब सहम जाते,
चुपचाप—
जैसे दीवार में लगी कीलें,
हिल भी नहीं सकतीं।
छोटी-छोटी बातें—
कमरे का बल्ब बंद करना भूल जाना,
माँ का खाना बनाने में देर होना,
या उनकी बात एक बार में न समझना...
बस, इतना काफ़ी था।
आँखें लाल,
आवाज़ ऊँची,
जैसे कोई तूफ़ान
कमरे में घूमता हुआ।
हम भाई-बहन
एक-दूसरे को देखते—
मन में उबलता लावा,
पर होंठ सिले हुए।
कभी मन करता,
चीख़कर कह दें सब,
जो बरसों से दबा रखा है।
पर डर,
जैसे कोई अदृश्य दीवार,
रोक लेता था।
पिताजी का अपमान—
सोचकर ही
साँस रुक जाती थी।
फिर, थोड़ी देर बाद,
तूफ़ान थम जाता—
पिताजी शांत,
जैसे कुछ हुआ ही न हो।\
कभी-कभी
वे हमारे पास आते,
कुछ कहने की कोशिश करते...
पर क्या कहें?
उन्हें भी नहीं पता,
हमें भी नहीं पता।
हमारे बीच
एक अजीब-सी ख़ामोशी—
जैसे कोई भूली हुई भाषा।
हँसना—
उनके सामने
जैसे कोई अपराध।
बातें—
बस ज़रूरी,
जैसे काम, पढ़ाई, दवाई...
उससे ज़्यादा
कुछ नहीं।
माँ—
जैसे एक पुल
हमारे और पिताजी के बीच।
सारी बातें
उनके ज़रिए,
जैसे कोई चिट्ठी
एक घर से दूसरे घर।
कभी-कभी,
रात में,
सोचता हूँ—
माँ नहीं रहीं तो...?
एक ख़ालीपन,
जैसे अँधेरे में
रास्ता खो गया हो।
पिताजी और हम
कैसे रहेंगे?
क्या बोलेंगे?
एक गहरी दरार
जो सालों से
बढ़ती ही जा रही है।
शायद
अब ये कभी नहीं भरेगी—
जैसे सूखी नदी का तल
बस रेत और पत्थर...
और हम,
किनारे पर खड़े,
बस देखते हुए,
चुपचाप,
हमेशा की तरह…
रचना शेयर करिये :